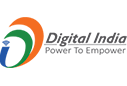भविष्य का दृष्टिकोण और आनुपातिक संकल्प
- मध्यस्थता के बारे में जागरूकता फैलाने के संबंध में:
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अनुसार, अब न्यायालयों पर यह वैधानिक दायित्व है कि जब किसी विवाद में समझौते का तत्व हो, तो न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे। इसके लिए यह आवश्यक है कि मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के निपटारे के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। हम इस वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के बारे में पक्षों को सूचित करने के लिए समन/नोटिस के साथ मध्यस्थता ब्रोशर भेजने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। जिला, ब्लॉक, तहसील स्तर पर और हमारे राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी सम्मेलन, सेमिनार और कानूनी सहायता शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव है, ताकि वादी, वकील और न्यायिक अधिकारी मध्यस्थता तकनीकों की उपयोगिता के प्रति संवेदनशील हो सकें और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के इस अभिनव तरीके का उपयोग कर सकें।
- मध्यस्थों और रेफरल न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के संबंध में:
हमने पाया कि न्यायिक अधिकारियों/वकीलों को मध्यस्थ बनने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करना मध्यस्थता केंद्रों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा उच्च न्यायालय निम्नलिखित के प्रशिक्षण के लिए पहल कर रहा है-
- रेफरल जज/समन्वयक
- मध्यस्थ/वकील
- मध्यस्थता केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे के संबंध में:
हमारा मानना है कि मध्यस्थता केंद्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचा होना चाहिए, ताकि मध्यस्थता कार्यवाही के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। इसके लिए हम पर्याप्त बजट की उपलब्धता की तलाश कर रहे हैं।
उपरोक्त प्रस्तावों/विचारों को क्रियान्वित करने तथा आम जनता को एडीआर की इस पद्धति का लाभ सुनिश्चित करने के लिए, हम चार आवश्यक स्तंभों अर्थात सरकार, बेंच, बार और वादी के बीच समन्वय स्थापित करके इसे पायलट परियोजना के रूप में लेने का प्रस्ताव कर रहे हैं और हमने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है।
जैसा कि ऊपर बताया गया है, यद्यपि नालसा के कहने पर प्रारम्भ में मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना हेतु 08 जिलों की पहचान की गई है, किन्तु राज्य के सभी 13 जिलों में न्यायिक संसाधनों के अन्तर्गत मध्यस्थता केन्द्र पहले से ही क्रियाशील हैं। उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में क्रमशः निम्न न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय में लगभग 1.66 लाख एवं लगभग 18,660 मामले लम्बित हैं। चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में लम्बित मामलों की संख्या कोई बहुत गम्भीर समस्या नहीं है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रथमतः केवल उन 08 जिलों में मध्यस्थता केन्द्र स्थापित किये जाएं, जहां अधिकतम मुकदमेबाजी है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश पर्वतीय जिलों में लम्बित मामलों की संख्या इतनी नहीं है कि मामलों के निपटारे हेतु मध्यस्थता एवं सुलह सहित वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रणाली लागू करने के लिए अत्यावश्यक एवं तत्काल उपाय की आवश्यकता हो। फिर भी, सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण विकसित मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना करके सम्पूर्ण राज्य में मध्यस्थता की अवधारणा को प्रसारित करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में, जिन 08 जिलों में लंबित मामले अन्य जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हैं, वहां मध्यस्थता केंद्रों के समुचित संचालन के लिए पर्याप्त आवास और समुचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। इस संबंध में भविष्य की संभावनाएं इस प्रकार हैं;
- यह सुनिश्चित करना कि मध्यस्थता केंद्रों के कुशल संचालन के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध हो, जिसमें स्वागत केंद्र, प्रतीक्षा कक्ष, पेयजल, शौचालय कक्ष आदि शामिल हों।
- यह सुनिश्चित करना कि मध्यस्थता केन्द्रों में प्रशिक्षित मध्यस्थ हों।
- यह सुनिश्चित करना कि इन मध्यस्थता केंद्रों को कुशल और वांछित तरीके से कार्यात्मक बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में मध्यस्थ उपलब्ध हों।
- यह सुनिश्चित करना कि माननीय न्यायाधीशों/रेफरल न्यायाधीशों को भी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए।
- जन शिक्षा और जागरूकता अभियान के माध्यम से पूरे राज्य में विशेष रूप से हमारे राज्य के दूर-दराज, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में ए.डी.आर. की अवधारणा को विकसित और बढ़ावा देना सुनिश्चित करना।
- हमारे राज्य के सभी 13 जिलों में मध्यस्थता केंद्रों का विस्तार और स्थापना करके इनके माध्यम से न्याय तक पहुंच बढ़ाना सुनिश्चित करना।
- समीक्षा:
जब तक किसी परियोजना के क्रियान्वयन की समय-समय पर निगरानी या समीक्षा नहीं की जाती, तब तक बाधाओं की पहचान नहीं की जा सकती और उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। इस संबंध में, हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे राज्य में कार्यरत मध्यस्थता केंद्रों की दक्षता की मासिक या द्विमासिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी की जाए। इससे हमें मध्यस्थता केंद्रों के प्रदर्शन और उपयोगिता का आकलन करने में मदद मिलेगी।
मध्यस्थता केंद्र की सफलता पूरी तरह से केंद्र को भेजे गए मामलों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह मामलों की गुणवत्ता, निपटाए गए मामलों की संख्या और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र को भेजे गए वादियों की संतुष्टि पर निर्भर करती है। राज्य के अधिकांश जिलों में लंबित मामलों की कम संख्या को देखते हुए, कई स्थानों पर पूर्ण विकसित मध्यस्थता केंद्रों को जारी रखने या न रखने की भी समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है या परियोजना के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए इसके गठन का पुनर्मूल्यांकन भी किया जा सकता है।
उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य में, अनेक बाधाओं के बावजूद, हमने मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारे राज्य में इस परियोजना को सफल बनाने के लिए निकट भविष्य में अनेक कार्य किए जाने हैं। मध्यस्थता निगरानी समिति के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति बीएस वर्मा इस मिशन और हमारे विजन को सफल बनाने के लिए लगातार परियोजना का मार्गदर्शन और निगरानी कर रहे हैं। मध्यस्थता परियोजना को सर्वांगीण रूप से सफल बनाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत क्षेत्र में अथक प्रयास कर रहे हैं।